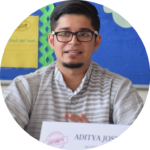

भारत को अपने संविधान पर गर्व है जो कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर गढ़ा और रचा गया है। भारतीय नागरिक कुछ मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करते हैं। भारत के संविधान ने भी देश के प्रचलित कानूनों के लिए एक शक्तिशाली आधारभूत संरचना तैयार की है। समय के साथ, कानूनी और विधायी प्रणालियां कुछ हद तक विकसित हुई हैं लेकिन, अभी भी बड़ी संख्या में कानून द्वारा प्रथाओं को मान्यता दी गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारत अस्पष्ट प्रथागत कानूनों के लिए अनजान नहीं है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत मनुस्मृति के मनमाने, अवैज्ञानिक कानूनों के द्वारा अक्सर अमानवीय और बर्बर होने की हद तक संचालित किया गया। मुंह और कान में गर्म सीसा डालना, सती प्रथा, समाज के मजबूत अलगाव पर आधारित जाति व्यवस्था ऐसे क्रूर कानूनों के केवल कुछ उदाहरण हैं।
भारतीय कानून के एक भाग के रूप में प्रथाएं
ऐसे ग्रंथों का प्रभाव अभी भी है और उन्हें समाज से पूरी तरह हटाया नहीं गया है। भारतीय संविधान प्रथाओं को कानून का एक हिस्सा मानता है। (भारतीय संविधान, अनुच्छेद 13, ) हालांकि, एक रिवाज को कानून के रूप में लागू होने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें है कि यह निरंतर उपयोग में होना चाहिए, तार्किक होने के साथ साथ इसे सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ नहीं होना चाहिए।
अधिकतर भारतीय व्यक्तिगत कानून जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम [1955] मुस्लिम शरीयत अधिनियम [1937] (मुस्लिम पर्सनल लाॅ (शरीयत) आवेदन अधिनियम,1937) उन निश्चित धर्मों की कई बरसों की मान्यताओं और व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। कानूनी ढांचे में रिवाजी कानून बताते हैं कि एक कानूनी प्रणाली समाज के भीतर से ही उभर रही है। परिणामस्वरूप, कुछ रीति-रिवाजों को नियम और कानून में समाहित कर दिया जाता है जो लोगों और समाज पर शासन करते हैं।समस्या तब पैदा होती है जब समय के साथ साथ ऐसे रिवाज़ आधारित कानूनों में बदलाव करने की जरूरत को महसूस नहीं किया जाता है। भारत एक विविधिताओं वाला मुल्क है जहाँ सभी नागरिक अपने धर्म को मौलिक अधिकार के रूप में प्रयोग करते हैं। इनमें से कई धार्मिक रीति-रिवाज समानता या नैतिकता की मूल अवधारणा के खिलाफ होते हैं।हालांकि, रिवाजी कानून समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन जब ये रास्ता दिखाने के एकमात्र सिद्धांत बन जाते है और बिना सोचे समझे इनका पालन किया जाता है, तब ये अक्सर कानून और व्यवस्था के लिए नाजुक और संकटपूर्ण स्थिति बना देते हैं।
इस बिंदु पर 2017 का एक मामला संदर्भ के रूप में हो सकता है जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने अमित जयसिंह सरैया विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य,( 728, 1996 मानदंड (3) 786) में जन्माष्टमी के त्योहार के दौरान “दही हांडी” प्रतियोगिताओं के लिए उम्र और ऊंचाई पर प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया था। देश भर के विभिन्न हिंदू समूहों ने इसकी व्यापक आलोचना की, इसकी तुलना हाल ही के मुस्लिम संगठनों द्वारा तीन तलाक को निरस्त करने की मांग के खिलाफ एक समान प्रतिरोध से की जा सकती है।
अवैज्ञानिक दर्शन, सांप्रदायिक राजनीति और व्यापक अशिक्षा पर आधारित मिथक इस तरह की गहरी धंसी प्रथाओं के कारण है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब सरकार अपने वोट बैंक को खोने के डर से ऐसे विषयों पर कोई मजबूत कदम नहीं उठाती हैं। भारतीय संसद द्वारा एक समान नागरिक संहिता की स्थापना न करने को भी इस तरह देखा जा सकता है जिसमें इसे कानूनी बाध्यता के बजाय एक सांप्रदायिक मुद्दा बना दिया गया है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित है। (भारतीय संविधान, अनुच्छेद 44)।
व्यक्तिगत कानून महिला अधिकारों के लिए बाधक
भारत के व्यक्तिगत कानूनों में सुधारों की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि इनमें से कई बहुत पुराने और मानव अधिकारों के उल्लंघन के समकक्ष है। यहाँ उल्लेख किया जा सकता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत निकाह हलाला की प्रथा एक ऐसी महिला जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया है, उसे वापस संबंध में आने से तब तक रोकती है, जब तक वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी एवं संसर्ग के बाद उस शादी को खत्म नहीं कर देती। ठीक उसी समय, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक मुस्लिम व्यक्ति को कई पत्नियां रखने की अनुमति देता है। ठीक उसी प्रकार पारसी पर्सनल लॉ पारसी महिला और उनके बच्चों को बिरादरी से निकाल देता है यदि वे पारसी धर्म से बाहर विवाह करती हैं।
पारसी कानून आगे संपत्ति के उत्तराधिकार को प्रतिबंधित करता है। यदि एक गैर-पारसी महिला का विवाह पारसी पुरुष से हुआ हो। ऐसे समय में जब भारतीय महिलाएं मोर्चा संभाल रही हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की अगुआई कर रही हैं। पुरुषों के साथ अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीत रही हैं, ऐसे समय में यह एक विडंबना है उन्हें अभी भी लैंगिक पूर्वाग्रहों के आधार पर “कमजोर” माना जाता है।
विभेदी कानून और भयानक परंपराएं केवल व्यक्तिगत कानूनों तक सीमित नहीं हैं। वर्षों से, एक धार्मिक स्थान में प्रवेश से संबंधित समस्याओं के कारण राजनीतिक उथल-पुथल हुई है। 2016 में, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने सफल आंदोलन का नेतृत्व किया जब उच्चतम न्यायालय ने, (कृष्णदास राजगोपाल, हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति, 19-09-2018 को प्राप्त किया)।हाजी अली दरगाह मुंबई, महाराष्ट्र में सभी महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी। हाल ही में, 2018 में, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय युवा वकील एसोसिएशन एवं अन्य विरूद्ध केरल राज्य डब्ल्यू पी. संख्या 373, एससी, 28/08/2018 भगवान अयप्पा सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र वर्ग की महिलाओं को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी। इस निर्णय को स्थानीय लोगों और मंदिर अधिकारियों से व्यापक आलोचना मिली। पुलिस के समर्थन से भी, उक्त आदेश के
बाद भी इस आलेख के लिखे जाने तक लागू नहीं किया जा सका है, एक और बेतुका रिवाज जिसने हाल ही में भारत में कानूनी बनाम सामाजिक उत्पीड़न का कोलाहल पैदा किया, उसका कारण है खतना जो कि भारत के वोहरा मुसलमानों के बीच प्रचलित है। चिकित्सा रिपोर्टों के अनुसार, इसने 75% बोहरा समुदाय कीलड़कियों को प्रभावित किया है[1]।।हैरानी की बात यह है कि भारत में एफजीएम को एक प्रथा के रूप में प्रतिबंधित नहीं किया गया है। एक जनहित याचिका में, अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया है कि यह आईपीसी धारा 320, 323, 324 और 325 के तहत अपराध है और आगे इस प्रथा को अपराध घोषित करते ही यह पोस्को अधिनियम के दायरे में आ जाएगी[2]।
डायन प्रताड़ना की प्रथा से निपटने में विधायी उपायों की विफलता
डायन प्रताड़ना एक और बर्बर प्रथा है जो मध्य भारत के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती है, जिसकी सूची में झारखंड का पहला स्थान है. इसका उपयोग महिलाओं के दमन के एक औजार के रूप में किया गया है, उन पर एक क्षेत्र में दुर्भाग्य लाने का आरोप लगाकर और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा का कारण बना या यहां तक कि फसल विफलताओं का दोष मढ दिया जाता था। डायन प्रताड़ना की पीड़ितों के प्रति हिंसा के कार्य को अकसर स्थानीय पंचायतों द्वारा समुदाय के लाभ के नाम पर उचित ठहरा दिया जाता है। इस प्रथा के कारण महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी के कारण कुछ राज्यों को डायन प्रताड़ना को रोकने हेतु कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जैसे कि बिहार में “डायन प्रथा की रोकथाम (डायन) अधिनियम “(1999)(डायन आचरण रोकथाम अधिनियम, 1999)। झारखंड में “जादू टोना रोकथाम अधिनियम” (2001) (डायन प्रताड़ना कार्य रोकथाम अधिनियम, 2001) “छत्तीसगढ़ टोनही” प्रताड़ना निवारण अधिनियम (2005) (छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005)। उड़ीसा की डायन प्रताड़ना रोकथाम अधिनियम” (2013), और “राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम (2015)” जैसे कानून अलग अलग राज्य विधायिकाओं द्वारा लाए गए है। आसाम विधानसभा ने असम डायन प्रताड़ना (प्रतिबंध, रोकथाम और संरक्षण) विधेयक,2015 में आजीवन कारावास की सजा निर्धारित है या फिर 5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ कारावास, यह अब तक का सबसे कठोर दंड है. हालाँकि, भारत के पास डायन प्रताड़ना के खतरे को रोकने के लिए कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, और आईपीसी की धारा 323, 354 और 382 के तहत उल्लेखित अपराधों के आधार पर सजा दी जाती है। डायन प्रताड़ना के भौगोलिक स्थानों के परीक्षण में रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति एक गहरी आस्था दिखती है जिससे रूढ़िवाद को बढ़ावा मिला।
खाप पंचायत महिला अधिकारों के लिए बाधक है:-
एक अन्य क्षेत्र जिसका उल्लेख करने योग्य है, वह है ग्रामीण क्षेत्र जिसमें विधायी पैठ की कमी है, जिसने स्व नियुक्त देव-पुरुषों, धार्मिक संस्थाओं जैसे न्यायिक निकायों को जन्म दिया है या खाप- पंचायतें।असंवैधानिक होने के अतिरिक्त ये स्व-नियुक्त न्यायिक संस्थाएं आनुपातिक मानदंड के रूप में सामाजिक मानदंड और स्थानीय परंपरा को बनाए रखते है। यहां तक कि बलात्कार और तेजाब हमलों जैसे मामलों में भी यह देखा गया है कि खाप या गांव के बुजुर्ग स्वत: ही फैसला दे देते हैं। यौन अपराधों या हिंसा से
बचे लोगों को उनके अपराधी के साथ स्थानीय ग्राम निकायों द्वारा “न्याय” के नाम पर शादी करा दी जाती है। इसके अलावा, इन फैसलों को लोगों द्वारा समुदाय से निर्वासित होने और परिवार में शर्मिंदा होने के भय और समुदाय से बाहर निकाले जाने के डर के कारण चुनौती नहीं दी जाती। निर्वासित होने के भय के कारण से ही ऑनर किलिंग जैसे अपराध में वृद्धि हुई है। ऑनर किलिंग एक ऐसे कृत्य को माना जाता है जिसके अनुसार जाति या अंतर-धार्मिक विवाह शर्म का विषय है।
एक कानून लाकर इस तरह के “विवेक की रक्षा करने वाली” खतरों को प्रतिबंधित करने में विधायिका की ओर से से निरंतर अज्ञानता के कारण न्यायपालिका को मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। खापों और अन्य समान निकायों के अतिरिक्त संवैधानिक कामकाज के मद्देनजर शीर्ष अदालत ने शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, 2010 की डब्ल्यू. पी. 231, एससी, 27.03.2018 कहा कि कोई भी सभा जो दो वयस्कों की सहमति के बीच विवाह की संस्था को वेग हीन करने का का इरादा रखती हो वह गैर संवैधानिक मानी जाएगी।
निष्कर्ष
हालांकि हर चीज का दोषारोपण सिर्फ और सिर्फ खाप पंचायतों पर ही करना गलत होगा, अधिकतम बार बाल विवाह और सम्मान हत्या से संबंधित मामलों को छोड़ दिया जाए तो यह परिवार ही है जो अपने बच्चे पर अत्याचार करता है। इसी तरह, बाल विवाह को अपराध की घोषणा करने वाले कानूनी प्रावधान होने के बावजूद अभी भी इसका पनपना जारी है और दर्ज होने से बचा रह जाता है। कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया है कि अगर हमें इस तरह की जघन्य गतिविधियों पर रोक लगाने वाला कानून मिल भी जाता है, तो भी यह मानसिकता है जिसे लोगों को बदलने की जरूरत है। इस प्रकार इन प्रतिगामी कानूनों को ग्रामीण भारत की
सामाजिक और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता के मद्देनजर भारी बदलाव की जरूरत है। जो केवल उच्च दर की शिक्षा और कानूनी प्रणाली की जागरूकता के साथ ही आ सकती है।
प्रतिगामी कानूनों और हिंसात्मक प्रथाओं के होते हुए भी यह मान लेना गलत होगा कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां रिवाज़ और परंपराएं विकास को रोकती हैं और देश उनके सामने विवश है।
भले ही कुछ मान्यताओं और धार्मिक व्यवहार को कुछ हद तक कानून के रूप में संचालित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद हमने एक लंबा रास्ता तय किया है।सती पर प्रतिबंध लगाना, महिलाओं को संपत्ति में एक समान हिस्सेदारी रखने का अधिकार देना, अतीत में परिवर्तन की दिशा में सभी छोटे कदम थे, अभी हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने (राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ समलैंगिकों को “तृतीय लिंग” के रूप में, 5 एससीसी 438, 508 (एससी,2014) में मान्यता दी, जिसके बाद 2018 में (अत्रि कर विरूद्ध भारत संघ,डब्ल्यू पी 2017 के नंबर 6151(डब्ल्यू), एससीसी, एससी, 16.03.2017) में धारा 377 को गैर कानूनी करने का ऐतिहासिक फैसला आया। यह स्वीकार करते हुए कि सदियों पुरानी मान्यताएं और अंधविश्वास किस तरह से विकास में बाधा बन सकते हैं, हमने एक अधिक समावेशी और आधुनिक भविष्य की ओर यात्रा शुरू की है।
वर्तमान में, भारत को जिस चीज की आवश्यकता है, वह है अल्पकालिक सुधारों के बरअक्स व्यापक सकारात्मक प्रभावों के साथ दीर्घकालिक समाधान। प्रथाओं और मानदंडों पर प्रतिबंध केवल सतही होंगे यदि उन्हें फलस्वरूप सुधारात्मक सामाजिक-आर्थिक उपायों के साथ लागू नहीं किया गया। हम खाप पंचायतों, मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश को वैध बना सकते हैं लेकिन हम रूढ़िवादी और आदिम मानसिकता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। यह समाज के भीतर से उभरता है और इसे निर्मूल करने का एकमात्र तरीका है कि व्यवस्थित खांचे की शिक्षा पर जोर दिया जाए, जागरूकता फैलाई जाए और झूठ का पर्दाफाश किया जाए।
(आदित्य जोशी विधि संकाय, दिल्ली विश्विद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्र है।
दीपक तैनगुरिया दिल्ली विश्वविद्यालय के एआरएसडी काॅलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक है)
-
(लक्ष्मीअंनत नारायण, शबाना दिलेर, नताशा मेनन, द क्लिटोरल हुड, ए कंटेस्टेड साइट, 17/09/2018 प्राप्त किया) ↑
-
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 ↑

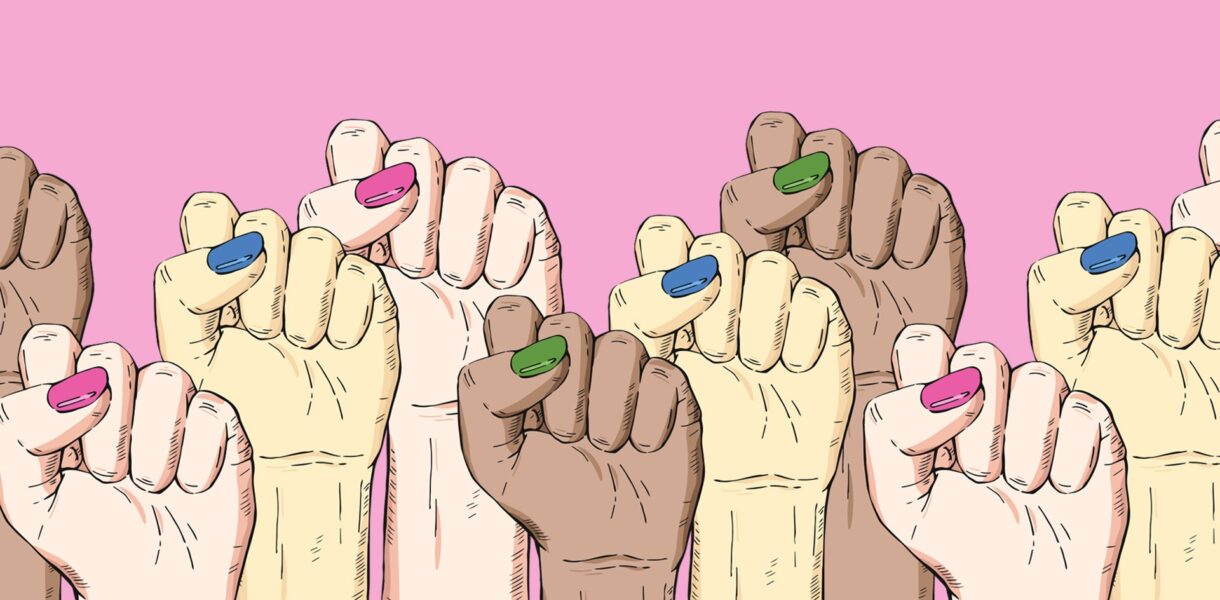



I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s
equally educative and interesting,
and without a doubt, you’ve hit the nail on the head.
The issue is something that too few men and women are speaking
intelligently about.
Now I’m very happy I found this in my search for something
concerning this.
Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your site?
My blog site is in the exact same niche as yours and my visitors would definitely benefit from some of the
information you present here. Please let me know if this ok with
you. Appreciate it!
Excellent beat ! I would like to apprentice
even as you amend your site, how can i subscribe for a
blog site? The account helped me a appropriate deal.
I have been tiny bit acquainted of this your broadcast
provided vibrant transparent idea
If you desire to obtain a good deal from this article then you have
to apply these strategies to your won web
site.
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video
to make your point. You obviously know what youre talking about, why
waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?